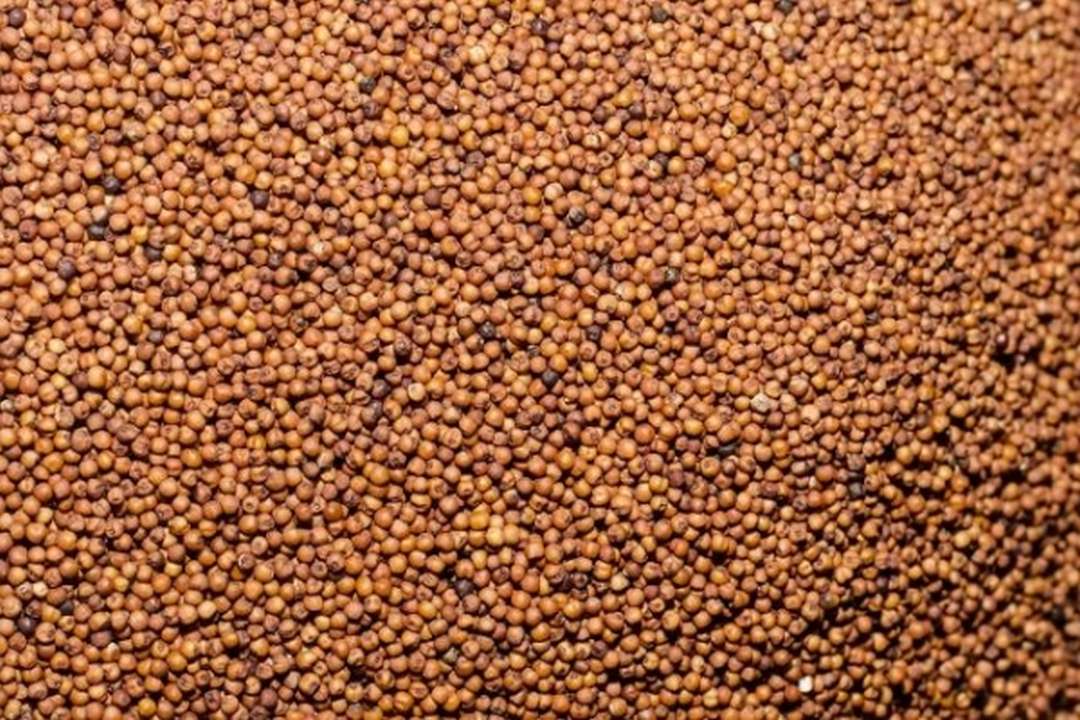VL-117, VL-204 and VL-115 हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध किस्में हैं।
VL Mandua 315: यह किस्म 105-115 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म फिंगर और गर्दन मरोड़ को सहनेयोग्य है।
VL Mandua 324: यह किस्म 2006 में जारी की गई है। इसके पौधे का कद 77-95 सैं.मी. होता है। यह किस्म 105-137 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके दाने बहुत हल्के कॉपर रंग के होते हैं। यह किस्म कुछ हद तक भुरड़ रोग को सहनेयोग्य है। इसकी औसतन पैदावार 6-10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।
VL Mandua 347: यह किस्म 2011 में जारी की गई है। इसके पौधे का कद 105-115 सैं.मी. होता है। यह किस्म 82-115 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके दाने बहुत हल्के कॉपर रंग के होते हैं। यह किस्म कुछ हद तक भुरड़ रोग को सहनेयोग्य है। इसकी औसतन पैदावार 6-10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।
VL Mandua- 352: यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों को छोड़ कर बाकी राज्यों में उगाई जा सकती है| यह 95-100 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 8-10 कुइंटल प्रति एकड़ है|
GPU 48: यह किस्म 2009 में जारी की गई। यह किसम 100-105 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म भुरड़ रोग की प्रतिरोधी है। इसकी औसतन पैदावार 12-14 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म पिछेती खरीफ और गर्मियों के मौसम में बोने के लिए उपयुक्त है।
GPU 66: यह किस्म 2013 में जारी की गई। यह भुरड़ रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 12-13 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।
GPU 67: यह किस्म 2010 में जारी की गई। यह किस्म 100-105 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म भुरड़ रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 12-14 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म पिछेती खरीफ और गर्मियों के मौसम में बोने के लिए उपयुक्त है।
KMR 301: यह किस्म 2011 में जारी की गई। यह किस्म 120 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बारानी क्षेत्रों में इसकी औसतन पैदावार 16-18 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और सिंचित क्षेत्रों में इसकी औसतन पैदावार 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म फिंगर और गर्दन मरोड़ को सहनेयोग्य है।
PES 400: यह 98-102 दिनों में तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 8 क्विंटल प्रति एकड़ है| यह जल्दी पकने वाली किस्म है और भुरड़ रोग की प्रतिरोधक है|
PES 176: यह 102-105 दिनों में तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 8-9 क्विंटल प्रति एकड़ है| इसके बीज भूरे रंग के होते है और भुरड़ रोग की प्रतिरोधक है|
KM-65: यह 98-102 दिनों में तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 8-10 क्विंटल प्रति एकड़ है|
VL 146: यह 95-100 दिनों में तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 9-10 क्विंटल प्रति एकड़ है| यह भुरड़ रोग की प्रतिरोधक है|
VL 149: यह 98-102 दिनों में तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ है| यह बहुत अनुकूल, अगेती और भुरड़ रोग की प्रतिरोधक किस्म है|
VL 124: यह 95-100 दिनों में तैयार हो जाती है| इसकी औसतन पैदावार 10 क्विंटल प्रति एकड़ है| यह बीज और चारे के लिए बढ़िया किस्म है|
VR 708: यह सूखे को सहनयोग किस्म है| यह सारे प्रांतो में उगाई जा सकती है|
Akshya
PES 110
PR 202
JNR 852
MR 374